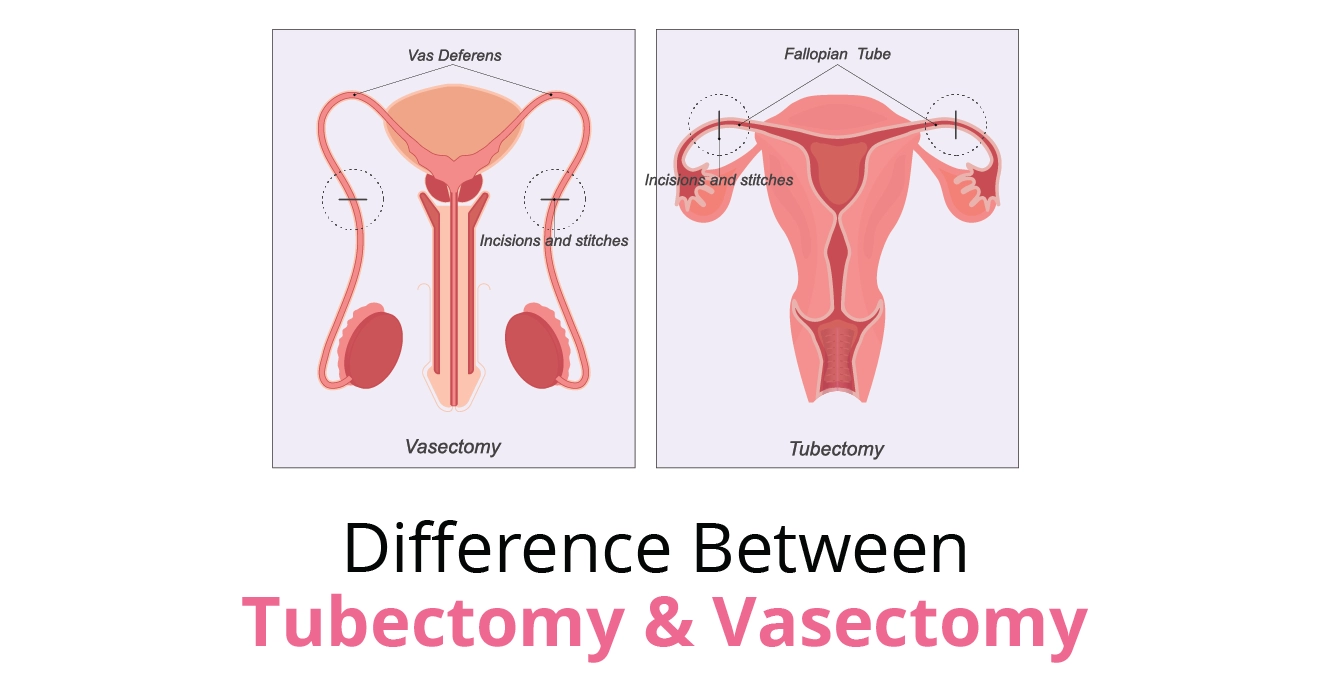आनुवंशिक विकार क्या है? Genetic Disorder Meaning in Hindi

Table of Contents
आनुवंशिक विकार क्या है?
जो बीमारियां माता-पिता या करीबी रिश्तेदारों से जीन के द्वारा शिशु में आती हैं उन्हें मेडिकल भाषा में आनुवंशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर (Genetic Disorder) कहते हैं। एक जीन में बदलाव भी जन्म दोष का कारण बन सकता है जैसे कि दिल से संबंधित दोष आदि। इस स्थिति को एकल जीन विकार भी कहते हैं और यह परिवार में एक से दूसरे व्यक्ति में जाता है।
हालाँकि, सभी माता-पिता से उनके बच्चों में जीन का केवल आधा हिस्सा ही जाता यानी पास होता है। आमतौर पर यह एक जीन में गड़बड़ी यानी मोनोजेनिक डिसऑर्डर या एक से अधिक जीन में गड़बड़ी यानी मल्टीफैक्टोरियल के कारण हो सकता है। इसके अलावा, यह समस्या जीन में म्यूटेशन के साथ-साथ पर्यावरणीय कारकों के संयोजन के कारण भी पैदा हो सकती है।
आनुवंशिक विकार के प्रकार
आनुवंशिक विकार या अनुवांशिक रोग कई तरह के होते हैं जिसमें शामिल हैं सिंगल जीन इनहेरिटेंस, मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम एब्नॉर्मेलिटीज, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस।
सिंगल जीन इनहेरिटेंस
सिंगल जीन इनहेरिटेंस ऐसे विकार हैं जिसमें केवल एक जीन में दोष होता है। इसके उदाहरण में हनटिंग्टन रोग, सिकल सेल बीमारी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आदि शामिल हैं।
हनटिंग्टन रोक के लक्षणों में शारीरिक गतिविधियां अनियंत्रित और भावनात्मक गड़बड़ी होना शामिल हैं। इस बीमारी का उपचार संभव नहीं है। हालाँकि, कुछ दवाओं की मदद से इसके लक्षणों का प्रबंधन किया जा सकता है।
सिकल सेल बीमारियां की स्थिति में लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इसके लक्षणों में दर्द, संक्रमण, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम और स्ट्रोक शामिल हैं। सिकल सेल बिमारियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं निर्धारित करते हैं।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आनुवंशिक स्थितियों का एक समूह है जिसमें मांसपेशियों को नुकसान पहुचंता है और वे कमजोर हो जाती हैं। डीएमडी नामक जीन में गड़बड़ी के कारण यह समस्या पैदा होती है।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज करने के लिए फ़िलहाल कोई विधि उपलब्ध नहीं है। लेकिन जीवन की क्वालिटी में सुधार करने के लिए डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं।
मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस
मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर ऐसी स्थितियां हैं जिनका मुख्य कारण आनुवंशिक, जीवनशैली या पर्यारण के कारकों का संयोजन है। इस स्थितियों में दमा, दिल की बीमारी, डायबिटीज, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस आदि शामिल हैं।
दमा का इलाज करने के लिए डॉक्टर स्टेरॉयड और एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं निर्धारित करते हैं। साथ ही, अस्थमा वाला इन्हेलर और नेब्युलाइजर के प्रयोग का सुझाव भी देते हैं।
दिल को प्रभावित करने वाली बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एनजाइना, कोरोनरी धमनी की बीमारी, अनियमित दिल की धड़कन और एथेरोस्क्लेरोसिस आदि शामिल हैं।
इन बीमारियों का उपचार करने के लिए डॉक्टर जीवनशैली में बदलाव का सुझाव देते हैं, दवाइयां और मेडिकल प्रक्रिया या सर्जरी की मदद लेते हैं।
डायबिटीज का उपचार करने के लिए जीवनशैली में बदलाव लाने और स्वस्थ आहार एवं इंसुलिन की कुछ दवाएं लेने का सुझाव देते हैं।
सिजोफ्रेनिया का इलाज कई तरह से किया जाता है और यह आमतौर पर इस समस्या के लक्षणों और उनकी गंभीरता एवं मरीज की उम्र तथा समग्र स्वस्थ पर निर्भर करता है।
अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज मौजूद नहीं है। लेकिन इनके लक्षणों को कम और जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर कुछ ख़ास प्रकार की दवाएं निर्धारित करते हैं।
क्रोमोसोम एब्नॉर्मेलिटीज
क्रोमोसोम एब्नॉर्मेलिटीज यानी गुणसूत्र असामान्यताएं वो समस्याएं हैं जिसमें क्रोमोसोम प्रभावित होते हैं जैसे कि पर्याप्त क्रोमोसोम नहीं होना, अतिरिक्त क्रोमोसोम होना या ऐसा क्रोमोसम जिसमें किसी प्रकार की संरचनात्मक असामान्यता हो।
कोशिका के विभाजन होने पर जब कोई त्रुटि (Error) होती है तो क्रोमोसोम एब्नॉर्मेलिटीज की समस्या पैदा होती है। आमतौर पर ये त्रुटियां स्पर्म या अंडे में होती हैं। हालाँकि, ये गर्भधारण के बाद भी हो सकती हैं।
क्रोमोसोम एब्नॉर्मेलिटीज में डाउन सिंड्रोम और वूल्फ-हिर्स्चहॉर्न सिंड्रोम शामिल हैं। डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे के जीवन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टर की टीम उसे चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है।
वूल्फ-हिर्स्चहॉर्न सिंड्रोम का उपचार नहीं है। लेकिन फिजिकल या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सर्जरी, जेनेटिक काउंसिलिंग, विशेष शिक्षा या ड्रग्स थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में गड़बड़ी जैसी समस्या केवल माँ से ही उसके बच्चे में पारित होती है। वर्तमान में माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर का कोई उपचार मौजूद नहीं है। हालाँकि, लक्षणों के आधार पर डॉक्टर पोषण प्रबंधन, विटामिन सप्लीमेंट, एमिनो एसिड सप्लीमेंट और कुछ ख़ास दवाओं की मदद से लक्षणों को कम कर सकते हैं।
आनुवंशिक बीमारियों की सूचि
कुछ मुख्य आनुवंशिक बीमारियों के नाम नीचे दिए गए हैं:
- रंगहीनता
- ऑटिज्म
- प्रोजिरिया
- मलेडा रोग
- एपर्ट सिंड्रोम
- टॉरेट सिंड्रोम
- डाउन सिंड्रोम
- मोनीलिथ्रिक्स
- ब्रूगाडा सिंड्रोम
- ऐकार्डी सिंड्रोम
- गार्डनर सिंड्रोम
- कॉस्टेलो सिंड्रोम
- स्टिकलर सिंड्रोम
- एंजेलमैन सिंड्रोम
- विलियम्स सिंड्रोम
- नेल पटेला सिंड्रोम
- ड्युबोवित्ज सिंड्रोम
- लेस-न्यहान सिंड्रोम
- ट्यूबरस स्क्लेरोसिस
- डीओओआर सिंड्रोम
- ट्रेचर कोलिन्स सिंड्रोम
- स्केलेटल डिस्पलेशिया
- आनुवंशिक लिम्फेडेमा
- चर्म रोग (कुछ ममलों में)
- निद्रा रोग (कुछ मामलों में)
जेनेटिक टेस्ट के क्या फायदे और नुकसान हैं?
जेनेटिक टेस्ट की मदद से आप आनुवंशिक बीमारियों का पता लगा सकते हैं और जांच के परिणाम से शुरूआती उपचार विकल्पों का चयन कर सकते हैं। हालाँकि, कुछ लोगों को यह जांच करवाने के बाद पछतावा भी हो सकता है, क्योंकि इस टेस्ट के बाद उन्हें इस बात का पता चला जाता है कि उनके बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। साथ ही, इस जांच से एक परिवार के कई भेद भी खोले जा सकते हैं जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या आनुवंशिक विकार ठीक हो सकते हैं?
जीवनशैली और डाइट में सकारात्मक बदलाव लाकर जींस की सेहत में सुधार करके उनके बुरे प्रभावों को रोका जा सकता है।
जेनेटिक टेस्ट कैसे होता है?
जेनेटिक टेस्ट में रक्त का सैम्पल लेकर उसका परीक्षण किया जाता है। जाँच के दौरान इस बात का पता लगाया जा सकता है कि माता या पिता में ऐसा कौन सा जीन मौजूद है जो उनके होने वाले बच्चे को जेनेटिक बीमारी दे सकता है। जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने होने वाले बच्चे को जेनेटिक विकार से बचा सकते हैं।
जेनेटिक टेस्ट कब करवाना चाहिए?
अगर आप या आपके पार्टनर के परिवार की पीढ़ियों से जेनेटिक बीमारियां जैसे कि स्तन या ओवेरियन कैंसर, मोटापा, पार्किंसस, सीलिएक या सिस्टिक फाइब्रोसिस चले आ रहे हैं तो ऐसे में आपको जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहिए।
Our Fertility Specialists
Related Blogs
To know more
Birla Fertility & IVF aims at transforming the future of fertility globally, through outstanding clinical outcomes, research, innovation and compassionate care.
Had an IVF Failure?
Talk to our fertility experts

 Our Centers
Our Centers